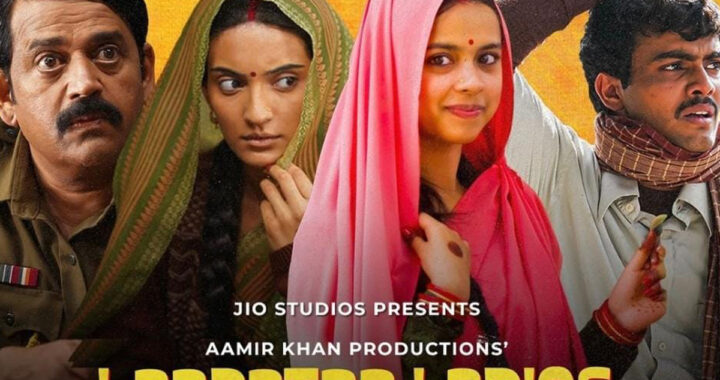यादों के गलियारे से : श्री 420 ( Shri 420 )
1 min read
filmania entertainment
-मुन्ना के. पांडेय
पचास का दशक हिंदी सिनेमा के इतिहास में ‘उम्मीदों भरा जमाना’ कहा जाता है. उस समय एक नया-नया आज़ाद हुआ मुल्क भविष्य की ओर एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहा था. यही वह समय था, जब भारतीय सिनेमा के दो बड़े नाम गुरुदत्त और राज कपूर उभरकर लगभग एक ही साथ रजतपट पर आए. इन दोनों के माध्यम एक थे, पर राहें यानी किस्सागोई अलहदा. गुरुदत्त जहाँ ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है’ से तत्कालीन व्यवस्था को एक अलग आलोचनात्मक तरीके से देख रहे थे, वहीं राज कपूर नेहरूवियन समाजवादी मॉडल को बहुत आशावादी नजरिये से देख रहे थे. यही वजह थी कि नेहरू के इस आइडिये/सपने का सटीक चित्रण राज कपूर की फिल्मों में पूरे विश्वास के साथ दिखाई दे रहा था. shri 420 इसका जीवंत उदाहरण है.
उस समय के सिनेमा के बारे में सुनील खिलनानी ने लिखा है -पचास के दशक में हुए बम्बई के चित्रण ने भारत से जुड़ी एक खास तरह की अवधारणा का प्रतिनिधित्व किया. राज कपूर और गुरुदत्त जैसे अभिनेता निर्माता-निर्देशकों की पीढ़ी और ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे वामपंथी पटकथा लेखकों ने अपनी प्रतिभा से भारत के जिस राष्ट्रवादी बिम्ब को फ़िल्म में मंचित किया और जिसके गीत गाये, वह साफ तौर पर नेहरू के विचार से प्रभावित लगता था.’यह फ़िल्म एक बेरोजगार नौजवान, गरीब शिक्षिका की कहानी भर नहीं रह जाती बल्कि बरास्ते महानगर बम्बई को उसकी संरचना और तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में एक औद्योगिक शहर को नए आज़ाद मुल्क की जन भावनाओं की पृष्ठभूमि में देखने की बाध्यता भी पैदा करती है. नायक राजू एक बीए पास नौजवान है, जो एक छोटे शहर इलाहाबाद से बम्बई जैसे बड़े शहर में कुछ करने के लिए आता है. शहर की ओर पलायन एक संभावना को लेकर आता है. अवसरों की बहुलता के कारण है, विकास का जो चेहरा बम्बई में पहले से विराजमान था, वह उस परिधि से बाहर वास्तविक तौर पर गाँवों की ओर निकला ही नहीं था. यहाँ राजू को जल्दी ही यह पता लग जाता है कि महानगर में अच्छी तालीम और ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों की कोई कद्र नहीं. राजू (राज कपूर) महानगर में गरीब स्कूल मास्टरनी विद्या (नरगिस) से प्यार करता है और माया (नादिरा) के चक्कर में आकर, सेठ सोनाचन्द धर्मानंद (नेमो) के साथ परिस्थितिवश मिलकर ‘चार सौ बीसी’ कर पैसा बनाता है. सेठ द्वारा दिखाए गए 100 रुपये में मकान का लालच दरअसल आज़ादी के बाद की वह छवि था, जहां बम्बई का स्थिर और सार्वदेशिक चरित्र विभाजन के बाद हिल सा गया था, कई हजार शरणार्थियों का जत्था इस शहर में आ गया था. (फुटपाथ पर राजू की घुसपैठ याद कीजिये). shri 420 इस शहर में पहले से स्थित अमीरों द्वारा पूरे हाशिये के बेघरों को सौ रुपये में मकान का लालच देकर लूटने का प्लान बनाने और नायक द्वारा अंत में विद्या और गंगा मैया (केलेवाली दिलवाली ललिता पवार) के प्रभाव और सहयोग से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर, अपनी दुनिया में लौट आने की कथा है. जहाँ तक विचार और कथातत्व की समानता का प्रश्न है, राज कपूर निर्देशित shri 420 और इसी फ़िल्म के लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास निर्देशित ‘शहर और सपना’ दोनों फिल्मों में रहने वाले गरीबों को मकान का लालच दिखाकर लूटने की कथा कही गयी है. यह फ़िल्म समाज के हाशिये के लोगों की आकांक्षाएं और संघर्ष तथा इनको अपने टूल्स की तरह प्रयोग करते पूंजीपतियों की कथा कहती है. परंतु अंत अपने तमाम इच्छाओं पर स्वयं ही निर्णय लेकर (हृदय परिवर्तन) वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट आने तथा नैतिक मूल्यों की रक्षा की नाटकीय प्रस्तुति करता है. इसमें दो राय नहीं कि फ़िल्म में किरदारों के नाम भी प्लाट के अनुसार ही हैं. ताकि फ़िल्म का कथ्य और संदेश शत-प्रतिशत दर्शकों तक पहुँच सके. हम जब पात्रों के इस संयोजन पर ध्यान देते हैं, तब पाते हैं कि साधारण, ईमानदार राजू विद्या, गंगा मैया और अपने ईमान से दूर होकर राज बनता है, जालसाज बनता है पर वह अपने इस बदलाव पर अंदर से खुश नहीं है. वह फिर से इनका साथ पाने पर वापिस सच्चाई की ओर लौट आता है.

इस फ़िल्म के गाने बेहद मशहूर हुए और आज भी हैं. मेरा जूता है जापानी यानी इंग्लिस्तानी पतलून, जापानी (फटे) जूतों और लाल रूसी टोपी में नेहरू के विचारों का यह ग्रेजुएट बेरोजगार युवक गाँव से संभावनाओं की तलाश में सपनों के शहर की ओर जाता है, वहाँ जीवन और देश की सच्चाइयाँ उसके आदर्शवादी मन और सोच को बदलने और 420 बनने पर मजबूर कर देते हैं. इस फ़िल्म के दो तीन महत्व के दृश्य है जिन पर संक्षेप में बात करनी जरूरी है. सेठ सोनाचन्द धर्मानंद की हवेली से ठीक सटे झुग्गी वालों का डेरा और वहाँ का एक संवाद ‘यह फुटपाथ एकदम नरम, बिल्कुल स्पेशल, ठीक सेठ सोनाचन्द धर्मानंद के महल के नीचे’ दरअसल आधुनिकता द्वारा दिखाए सपने की मौत है, जिसके सहारे नव स्वतंत्र भारत देश के नागरिक पुरातन व्यवस्था की गैर-बराबरियों के चंगुल से निकल जाने का मार्ग तलाश रहे थे. नेहरू एक समाजवादी और औद्योगिकीकरण वाले मुल्क की बात कर रहे थे परंतु यह वर्ग उनकी इस योजना में, खांचे में मिसफिट था.

नेहरू के जमाने में जो केंद्र राज कपूर अपनी फिल्मों में लाये वह कीमतों में बदल गयी. आज़ादी के बाद जो स्वप्न आदमी ने देखे वह दुःस्वप्नों में बदल गए. वैसे पर्यावरणविद एडवर्ड गोल्डस्मिथ ने लिखा है – आगामी दो दशकों में आधे से अधिक आबादी झुग्गियों में रहेगी, इसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है. झुग्गियाँ दरअसल तीसरी दुनिया के आधुनिकता की प्रथम दृष्टतया चिन्ह है. ऐसा एक और दृश्य चौपाटी और मंजन वाले दृश्य का भी है. चौपाटी का यह दृश्य जनता की दुखती रग और जीवन की बुनियादी जरूरत की नंगी तस्वीर सामने ले आता है. याद रहे यह सारा खेल, सारे सवालात औद्योगिक शहर की नाक के नीचे उठाये जा रहे हैं, जहाँ से देश की प्रगति का स्वप्न नीति-नियंताओं ने देखा है. सेठ का चरित्र शहर के उस क्रूर चेहरे का प्रतीक बनकर सामने आता है, जहां समस्या से जूझने की कवायद नहीं बल्कि ख्याली जुमले और खोखले आदर्शवाद का जुमला आमजन को दिया जाता है. नेहरूवियन मॉडल का यह नायक यह सवाल भी उठाता है कि पढ़े-लिखे काम के लिए ठोकरे खाते युवा वर्ग के लिए कोई सार्थक रास्ता नहीं तैयार किया जाएगा तब वह निश्चित ही एक ऐसी राह चुनेगा जो राष्ट्र और समाज ही नहीं बल्कि खुद उस युवक के लिए भी गलत ही होगा. फ़िल्म का अंतिम दृश्य आत्मालोचन का दृश्य है जहाँ नायक खलनायक के सवाल जवाब हैं जनता के जाग जाने का अद्भुत दृश्य है. यह अकेला दृश्य है जब सेठ घबराता है. और अंत में जनता घर का दृश्य जनता के मन में भविष्य के आशावाद का बीजारोपण है. हो भी क्यों ना आखिर ऐसे ही स्वप्नों से दुनिया कायम है. राज कपूर ख्वाजा अहमद अब्बास, शैलेन्द्र, साहिर, गुरुदत्त सब बेहतर दुनिया के स्वप्नदर्शी ही तो थे. वह जानते थे कि ‘स्वप्न तो देखने ही होंगे, देखे जा रहे हैं. भविष्य स्वप्न तो कोहेकाफ का कुकूनस पक्षी है, जो अपनी राख से बार-बार जन्म लेता रहता है और लेता रहेगा’. किस्से और भी है फिर कभी
(संदर्भ के लिए प्रयुक्त पुस्तकें- भारतनामा, सुनील खिलनानी/भारतीय सिनेमा का अंतः करण/यूटोपिया की जरूरत, सँ.रमेश उपाध्याय, संज्ञा उपाध्याय)