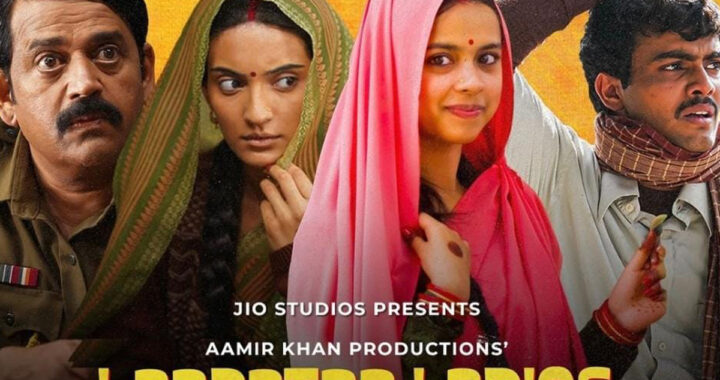फिल्मीनामा: दो बीघा जमीन
1 min read
-चंद्रकांता
हो जाये अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहाँ.
खाते, खवाई, बीज ऋण से हैं रंगे रक्खे जहाँ॥
आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में.
अधपेट खाकर फिर उन्हें है काँपना हेमंत में॥
विमल रॉय की क्लासिक फ़िल्म ‘दो बीघा जमीन’ (1953) किसान होने की इसी छटपटाहट को उघाड़ती है. फ़िल्म की शुरूआत आकाल की पृष्ठभूमि से होती है. अकाल से जूझते हुए गाँव में अचानक बादल गरजते हैं और देखते ही देखते बरसात होने लगती है. घोर नाउम्मीदी में बादलों का आसमान में घिर आना ग्रामीण किसान समाज में उत्सव बन जाता है. पूरा गांव गीत गा रहा है ‘हरियाला सावन ढोल बजाता आया, धिन तक तक मन के मोर जगाता आया’, यह गीत बड़ा ही कर्णप्रिय है. गांव वाले झूम रहे हैं बच्चे खुश हैं पुरुष अपनी मेहरारू को छेड़ रहे हैं. आपको याद होगा आशुतोष गोवारिकर की लगान (2001) का गीत ‘ घनन घनन घन घिर आए बदरा’ भी इसी थीम पर बुना गया था.
फ़िल्म का कथानक ऋण में आकंठ डूबे किसान के संघर्ष के इर्द गिर्द बुना गया है. बंगाल के किसी गाँव में एक किसान है शंभू महतो , जो अपने बूढ़े बीमार पिता (नाना पालशिखर) पत्नी पारो (निरूपा रॉय) और बेटे कन्हैया (रतन कुमार) के साथ बसर कर रहा है. गांव के जमींदार ने अपनी जमीन पर मिल फैक्टरी ‘दी ग्रेट जनता मिल्स लिमिटेड’ बनाने का फैसला लिया है. उसकी जमीन के बीच में दो बीघा टुकड़ा शम्भू का भी है. ठाकुर जमींदार शंभू को उसकी जमीन के बदले मिल के बन जाने पर पक्की सड़क बनने, बिजली आने और कर्जा माफ करने का लालच देता है.लेकिन जमीन को माँ का दर्जा देने वाला शंभू इससे इंकार कर देता है.
जमींदार लिए गए कर्जे के बदले शंभू की जमीन हड़पने की कोशिश करता है. मामला कचहरी तक पहुंचता है. लगान चुका दिए जाने की रसीद अनपढ़ शम्भू के पास है नहीं और ऋण के कागजों पर उसका अंगूठा लगा है. सब सामान इकट्ठा कर भी वह रुपये 235 का कर्ज नहीं चुका पाता. अदालत तीन महीने का वक़्त देती है. शंभू के पास जो कुछ होता भी है वह भी कोर्ट कचहरी में लग जाता है. अंततः शंभू अपने बीमार पिता और गर्भवती पत्नी को छोड़ कन्हैया के साथ काम की तलाश में कलकत्ता शहर जाता है और वहां रिक्शा चलाने का काम करता है.
फ़िल्म में एक दृश्य है जहां एक प्रेमी युगल की मनोरंजन भरी स्पर्धा में शंभू अपना रिक्शा लेकर दौड़ता है ..खूब दौड़ता है..और तेज दौड़ता है और फिर दुर्घटना हो जाती है. फिल्मकार ने यहां एक बेहतरीन समानांतर खींचा है. शंभू की यह दौड़ हमारे सपनों की दौड़ है. बलराज साहनी ने अपने किरदार का इतना उम्दा निबाह किया है कि बलराज साहनी और शम्भू में कोई अंतर नहीं रहता.शंभू बहोत बीमार है लेकिन कन्हैया के जुगाड़ किये चोरी के पैसे लेने से मना कर देता है. गरीबी के क्रूरतम दिनों का सामना इतने औदात्य से करना, गज़ब का फिल्मांकन है.शंभू का बेटा कन्हैया जिसकी उम्र लगभग आठ-दस साल की है लेकिन उसकी पहली चिंता परिवार का कर्ज उतारने की है इसलिए अपने बीमार पिता को भूखा देख वह खुद भी भूखा रहता है.
वो आदमी नहीं मुक्कमल बयान है
माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है. (दुष्यंत)
दो बीघा जमीन फ़िल्म का एक और पक्ष है पति-पत्नी के संबंध की खूबसूरती. पति-पत्नी के बीच छेड़खानी और हंसी ठिठोली का यह निजी स्पेस कॉपरेट जीवन में कम हुआ है. अनपढ़ पारो मिश्राईन (मीना कुमारी) के पास चिट्ठी लिखवाने जाती है और शंभू के लिए ‘बचुआ के बापू’ संबोधन का इस्तेमाल करती है. इस संबोधन का समाजशास्त्र अपनी जगह है लेकिन इसमें सहजता और मिठास है.इस मिठास से परिचित होने के लिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा देखना चाहिए. फ़िल्म में पति का पत्नी के लिए प्रेम बेहद ठोस है क्लाइमेक्स से पहले जब पारो भी कलकत्ता पहुंच जाती है और दुर्घटना का शिकार होती है तो उसकी जान बचाने के लिए शंभू ऋण चुकाने के लिए जमा की गई रकम पारो के इलाज पर खर्च करने को तवज्जो देता है.
यह फ़िल्म सलिल चौधरी की कहानी ‘रिक्शावाला’ पर आधारित है.फ़िल्म में उनका संगीत भी बेहद कर्णप्रिय है. दो बीघा जमीन के संगीत में यथार्थ की गंध है. विमल राय की इस फ़िल्म में ऋषिकेष मुखर्जी सहायक निर्देशक थे फ़िल्म की पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी. फ़िल्म में इस्तेमाल शब्द धरती कहे पुकार के, पाकेटमार और 24 चौरंगी लेन पर बाद में फिल्में भी बनी. फ़िल्म की बुनावट बहोत अच्छी है और कहानी में बेहतरीन फ्लो है. फ़िल्म का अंतिम दृश्य बेहद विदारक है, मन जो झंझोड़ कर रख देने वाला.
कन्हैया – मां, वह देखो जहां से धुआं उठ रहा है ठीक वहीं अपना मकान था.
पारो – और वहां मेरी रसोई थी.
शंभू थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मुट्ठी में भरता है चौकीदार आकर पूछता है क्या चुरा रहा है!! शंभू मुठ्ठी खोलता है और मिट्टी बिखरकर उसके हाथों से गिर जाती है. फिर तीनों वहां से चल देते हैं. कामगार को अपनी ही जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी पर भी हक़ नहीं. ऋणग्रस्त किसानों का ऐसा ही दुःख भरा चित्र महबूब खां ने ‘मदर इंडिया’ में भी खींचा है.
हमें याद नहीं किसानों या आदिवासियों-वंचितों की समस्या पर इधर कुछ समय में मुख्यधारा की कोई फ़िल्म बनी हो. आप सभी मित्रों से यह निवेदन है की नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के इस दौर में आपके बच्चों को दो बीघा जमीन, जागते रहो, बूट पॉलिश, दो आंखें बारह हाथ और दोस्ती जैसी संजीदा फिल्में भी दिखाइए. इनमें यथार्थ को दिखाने के लिए अश्लीलता और अनावश्यक भौंडी हिंसा का सहारा नहीं लिया गया है. मजदूर और किसान भी हमारी दुनिया का सच है बच्चों को ऐसा सिनेमा भी दिखाइये ताकि उनकी तबियत इस यथार्थ को सूंघ सकने की बन सके.